भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले के राजनीतिक-आर्थिक असर पर 8 नवंबर से ही बात हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों की कानूनी मान्यता खत्म होने का ऐलान किया था और कहा था कि आधी रात से यानी लोगों को भरोसे में लेने के कुछ घंटे बाद से ही ये नोट रद्दी के टुकड़ों में बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान वित्त मंत्री से कराने के बजाय स्वयं ही किया, इसीलिए इसमें नाटकीयता का पुट भी आ गया। इसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला चल निकला, जिसमें प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी। आम आदमी ने, उद्योग ने और कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने भी इस निर्णय को सराहा। अन्य विरोधियों ने इसकी निंदा की और कुछ ने तो इस कदम के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतारने की धमकी भी दे डाली। बमुश्किल दो सप्ताह बाद शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मसले पर व्यवधान पड़ता आया है। जाहिर है कि अभी मामला निपटा नहीं है।
विमुद्रीकरण का फैसला तीन बड़े कारणों से लिया गयाः पहला, काले धन की अर्थव्यवस्था, जो बड़े नोटों पर ही फली-फूली थी; दूसरा, जबरदस्त भ्रष्टाचार, जो समानांतर अर्थव्यवस्था की ताकत पर ही चलता है और तीसरा जाली नोट, जिनसे आतंकवाद को आर्थिक मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में इन्हीं मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। इसमें हैरत नहीं है कि इस कदम से भारी असुविधा (पिछले हफ्तों में देश भर में बैंकों में पसरी अव्यवस्था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है) झेलने के बावजूद आम आदमी ने इसे समर्थन दिया है क्योंकि उसे लगता है कि सरकार ने अवैध धन इकट्ठा करने वाले धनी लोगों पर, भ्रष्ट और भ्रष्ट करने वालों पर और आतंकवाद के अभिशाप पर आखिरकार चोट कर ही डाली है। लेकिन एक चौथा पहलू भी है और वह है चुनाव लड़ने में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध धन खत्म होना। कुछ महीनों के भीतर ही विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं और भाजपा के विरोधी रानीतिक दल यह सोचकर परेशान है। कि रकम का इंतजाम कहां से किया जाएगा। इसी बदहवासी में उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर अपने लिए रकम का ‘इंतजाम’ करने के इरादे से अपने लोगों को ‘इस कदम की सूचना पहले ही दे देने’ का आरोप लगाया है। इसीलिए हकीकत यह है कि जिन राजनीतिक दलों ने सरकार के इस फैसले के कारण आम आदमी को बहुत अधिक तकलीफ होने की और इसे वापस लिए जाने की बात कहते हुए इस कदम की निंदा की है, असल में वे राजनीतिक फायदे के लिए काले धन की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने तो यह हास्यास्पद दावा तक कर दिया कि वित्तीय संकट के समय काले धन की अर्थव्यवस्था ने ही देश को बचाया था! ‘अंदरखाना सूचना’ दिए जाने की बात पर भरोसा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मीडिया की खबरों में पिछले दिनों बताया गया है कि सरकार ने पूरी तरह गोपनीयता बरती थी और मुट्ठी भर अधिकारियों को ही इस योजना के बारे में पता था। सरकारी बैकों के प्रमुखों को और अधिकतर केंद्रीय मंत्रियों तथा वरिष्ठ नौकरशाहों को भी इसकी खबर नहीं थी। लेकिन राजनीतिक हायतौबा ने एक काम तो कर ही दिया। उसके कारण एक बार फिर चुनाव प्रणाली, विशेषकर चुनावों के धन के इस्तेमाल को सुधारने की जरूरत पर ध्यान लौट आया है। प्रधानमंत्री ने संसद का सत्र आरंभ होने से सप्ताह भर पहले सर्वदलीय बैठक में सरकारी रकम से चुनाव कराए जाने की जोरदार हिमायत की ताकि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार का मुकाबला हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि विमुद्रीकरण पर बातचीत से यह “सकारात्मक संदेश” जाएगा कि देश का राजनीतिक वर्ग जनता की भलाई के लिए एकजुट है। दिलचस्प है कि बैठक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने इस निर्णय का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से चुनावों के लिए सरकारी रकम के पक्ष में रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस विमुद्रीकरण के फैसले की सार्वजनिक आलोचना कर चुकी है और सड़कों पर उतरने की धमकी दे चुकी है।
सरकारी रकम से चुनाव कराने का प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव नया नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण अभियान के मौजूदा संदर्भ में इसकी अहमियत बढ़ गई है। सरकार यह संदेश देना चाहेगी कि सरकारी रकम पर चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके अभियान का ही एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में आने वाले महीनों में वह विमुद्रीकरण से आगे बढ़ना चाहती है। किंतु विमुद्रीकरण कार्यपालिका का निर्णय था, जो राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली (पिछली संप्रग सरकार में इच्छाशक्ति नहीं थी) कोई भी सरकार ले सकती थी। लेकिन सरकारी रकम पर चुनाव कराना पेचीदा मामला है, जिसके लिए सभी राजनीतिक खेमों में व्यापक सहमति जरूरी है - जो आसानी से नहीं हो पाएगी। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने कम से कम बातचीत तो शुरू की है, हालांकि यह किसी को नहीं पता कि बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। किंतु सरकारी रकम पर चुनावों के बारे में चर्चा करने से पहले यह जानना उचित रहेगा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने साल भर पहले इस मसले पर हुए दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन में क्या कहा था। सरकारी खर्च के विचार को स्वागत करते हुए उन्होंने आगाह किया था कि अगर चुनाव अभियानों में अवैध धन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूत कानून नहीं बनाया गया तो यह कदम नाकाम ही साबित होगा। उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि उम्मीदवारों के कुल खर्च में दलों तथा किसी तीसरे पक्ष द्वारा चुनाव क्षेत्र में किए गए खर्च को उम्मीदवारों के कुल खातों में जोड़ने पर कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने तथा उन्हें सार्वजनिक कर जुर्माना लगाए जाने से चुनाव क्षेत्र के स्तर पर कुल खर्च (चुनाव संबंधी खर्च) में कमी आ सकती है।” उन्होंने कहा कि चंदों पर नियंत्रण करने वाले मौजूदा नियम चुनावों में काले धन की आमद को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग को संदेह है कि सरकारी रकम चुनाव अभियान में काले धन के इस्तेमाल को कम किए बगैर रकम का एक और स्रोत और जरिया बन जाएगी। एक तरह से यह सही सोच वाले नागरिकों को चुनाव लड़ने से रोक सकता है...” राजनीतिक वर्ग और विशेषकर सरकार को इस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है।
इस बीच इस बात पर अलग-अलग नजरिये हैं कि सरकारी रकम पर चुनाव कराना कितना प्रभावी होगा। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका सहयोगी प्रकाशन द इकनॉमिक टाइम्स इस विचार को खारिज करते रहे हैं, लेकिन भाजपा (प्रधानमंत्री की प्रेरणा से) और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां सुझाव के पक्ष में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात पर अचरज जताया है कि घाटे वाले बजट से जूझ रही सरकार राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए धन कैसे दे सकती है। विमुद्रीकरण से इकट्ठा हुए धन का इस्तेमाल इसके लिए करना “हास्यास्पद” ही होगा क्योंकि इसका मतलब होगा सरकारी खर्च पर राजनेताओं के लिए और भी पैसा। अखबार ने 17 नवंबर के अपने संपादकीय में चेतावनी भी दी कि सरकारी मदद की व्यवस्था होने पर हर दूसरा संगठन केवल सरकारी रकम हासिल करने के लिए राजनीति में उतरने लगेगा। द इकनॉमिक टाइम्स ने 17 नवंबर के अपने संपादकीय में सरकारी खर्च पर चुनाव कराने को “बहुत खराब विचार” बताया था। उसने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों पर “इतना कम” सरकारी खर्च देखते हुए राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देने का सरकार का विचार ही अटपटा है। उसने सख्त लहजे में कहा, “सार्वजनिक संसाधनों को ऐसी आवश्यक सेवाओं की ओर मोड़ना चाहिए, उनसे दूर नहीं करना चाहिए और उसके लिए रकम देना अजीब है, जिसके लिए पहले ही ढेर सारी रकम मिलती है।” इस दलील में दो खामियां हैं। पहली, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सामाजिक क्षेत्रों के लिए जाने वाली रकम को चुनावों के लिए खर्च किया जाएगा। दूसरी, राजनीतिक दलों को जो ‘ढेेर सारी’ रकम मिलती है, उसमें बड़ा हिस्सा अवैध धन का होता है। जब सरकार इस पर चोट करेगी तो राजनीतिक दलों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रखने के लिए धन के पारदर्शी स्रोतों की आवश्यकता होगी।
हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने सरकारी फंडिंग के विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई थी तो वह राजग सरकार का प्रशासन का पहला राष्ट्रीय एजेंडा आगे ले जा रहे थे, जिसमें चुनावों में आमूल-चूल सुधारों का वायदा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसकी व्यावहारिकता जांचने के लिए 1999 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षमता में एक बहुदलीय संसदीय समिति गठित की थी। इसके अन्य सदस्यों में कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी शामिल थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए सरकार से रकम दिए जाने की पुरजोर सिफारिश की थी। लेकिन उसने यह भी कहा था कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा ‘राष्ट्रीय’ अथवा ‘राज्यस्तरीय’ दलों की मान्यता पाए हुए दलों तथा ऐसे दलों द्वारा सीधे उतारे गए उम्मीदवारों को ही सरकार से मदद मिलनी चाहिए। समिति का यह विचार भी था कि आदर्श रूप में चुनावों के लिए पूरी रकम सरकार से ही मिलनी चाहिए, लेकिन बजट की किल्लत आड़े आ सकती हैं। इसीलिए समिति के सदस्यों ने मोटे तौर पर यह माना कि आंशिक रकम देकर शुरुआत की जा सकती है यानी सरकार मान्यता प्राप्त पार्टियों के कुछ निश्चित खर्चों के लिए रकम खुद देगी। समिति ने कहा कि इस कदम का मकसद राजनीतिक दलों को अपना काम चलाने, अपने कार्यक्रम संचालित करने और चुनाव लड़ने के लिए बाहर से रकम लेने (मामूली सदस्यता शुल्क के अलावा) के मामले में हतोत्साहित करना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम सरकारी खर्च पर चुनावों की ही बात नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक दलों के कामकाज के लिए भी सरकारी रकम की बात कर रहे हैं। चुनाव तो इसका मामूली हिस्सा भर हैं।
समिति की सिफारिशों पर थोड़ा और विचार करना ठीक रहेगा क्योंकि इसने जो सुझाव दिए हैं, उनके साथ ही इस पर आगे बढ़ने की मांग शुरू की जा सकती है या वे आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। समिति ने लगभग 600 करोड़ रुपये के वार्षिक योगदान (उस समय के कुल 60 करोड़ मतदाताओं से 10 रुपये प्रति मतदाता की दर से) वाला अलग चुनाव कोष बनाने की सिफारिश की। इसमें केंद्र का तथा राज्यों द्वारा कुल मिलाकर उसके बराबर राशि का योगदान होगा। उसने यह भी कहा कि केवल उन्हीं पार्टियों को सरकारी रकम मिलेगी, जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए होंगे। समिति ने सुझाव दिया कि सरकारी रकम के लिए अर्हता वाली पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव अभियान हेतु वाहनों के लिए निर्धारित मात्रा में ईंधन, चुनावी साहित्य तैयार करने के लिए निर्धारित मात्रा में कागज और लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा के लिए एंप्लिफायर सिस्टम दिए जाएं, लेकिन प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए ऐसे अधिकतम 6 सेट दिए जाएंगे। इनमें से कुछ सिफारिशों को बाद के वर्षों में किसी न किसी रूप में लागू कर दिया गया है, लेकिन सरकारी आर्थिक मदद का अहम मसला अभी अनसुलझा ही है। उस समय उम्मीदवार के खर्च का अनुमान लगाने के तरीके पर भ्रम था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) की व्याख्या (1) के अनुसार उम्मीदवार के चुनाव के सिलसिले में राजनीतिक दल द्वारा किए गए किसी भी खर्च को उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा तय करते समय उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार निर्धारित सीमा के बाहर किए गए किसी भी खर्च को अपने राजनीतिक दल या संगठन द्वारा किए गए खर्च में दिखा सकता है। इससे खर्च पर नियंत्रण करने और पारदर्शिता लाने का मकसद ही पूरा नहीं होता है क्योंकि राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा अब भी अपारदर्शी होता है। 1999 में दिनेश गोस्वामी समिति ने इसे ठीक करने के लिए यह सुझाव दिया था कि व्याख्या (1) को निकाल दिया जाए। समिति ने कहा कि उम्मीदवार के राजनीतिक दल अथवा दोस्तों या संगठनों द्वारा अभियान पर किए गए खर्च पर नजर रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण यह व्याख्या उम्मीदवार और राजनीतिक दल दोनों को बच निकलने का रास्ता दे देती है। गोस्वामी समिति ने व्याख्या और भारतीय दंड संहिता की धारा 171(एच) के बीच विरोधाभास की ओर भी ध्यान दिलाया। धारा 171(एच) दलों अथवा संघों अथवा संगठनों को उम्मीदवार से अधिकार मिले बगैर चुनाव अभियान में किसी भी तरह का खर्च करने से रोकती है। इसलिए यदि उम्मीदवार को इस बात की जानकारी है तो चुनावी खर्च की कानूनी सीमाएं लांघने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
भारतीय विधि आयोग ने भी 1999 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ‘पूरी तरह’ सरकारी मदद तभी वांछित लक्ष्य है, जब राजनीतिक दलो को दूसरे स्रोतों से धन पाने से रोका जाए। इसने इंद्रजीत समित की इस सिफारिश से भी सहमति जताई कि बजट की किल्लत देखते हुए फिलहाल आंशिक आर्थिक मदद से शुरुआत अच्छी रहेगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उसने पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक ढांचे और खातों के रखरखाव, उनकी जांच और उन्हें समय से चुनाव आयोग के समक्ष पेश करने के लिए सबसे पहले नियामकीय ढांचा लागू करने की अनिवार्यता पर जोर दिया, जैसा चुनाव आयोग कई मामलों में कहता है। 2008 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी चुनावों में “अवैध और अनावश्यक रकम” का प्रवाह रोकने के लिए सरकार से आंशिक मदद का समर्थन किया था। किंतु संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2001 में सरकारी मदद के विचार पर उत्साह नहीं दिखाया, हालांकि वह इस सुझाव पर सहमत था कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियामकीय प्रक्रिया होनी चाहिए।
राजनीतिक दलों को सरकारी मदद के विचार से केवल भारत ही नहीं जूझ रहा है, दूसरे लोकतंत्र भी इस समस्या से रूबरू हुए हैं। फिनलैंड, इटली, इजरायल, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में इस विचार को लागू किया गया, जिसके मिश्रित नतीजे आए। उदाहरण के लिए इटली, इजरायल और फिनलैंड में तमाम उपाय किए गए, लेकिन सरकारी मदद मिलने से चुनावों के खर्च में अधिक कमी नहीं आई। इनमें से अधिकतर देशों में सरकारी खर्च के विरोध में यही दलील दी जाती है कि नागरिकों के स्वतंत्र संगठन होने के नाते राजनीतिक दल स्वतंत्र निकाय हैं और उन्हें वित्तीय बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करने वाले भारत में भी यही दलील दे सकते हैं।
उस समय सर्वदलीय समिति ने जो सिफारिशें की थीं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मोटे तौर पर सहमत थे। लेकिन झगड़ालू भारतीय राजनीति के कारण उन सिफारिशों को कानून का जामा नहीं पहनाया जा सका। अब देखना है कि उसी राजग खेमे से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ पाते हैं या नहीं क्योंकि राजनीति में 1999 से ज्यादा न सही, उतने खेमे तो आज भी हैं। अंतर एक ही है, मोदी बेशक गठबंधन की सरकार संभाल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में भाजपा के पास निर्णायक बहुमत है। शायद इस निर्णायक बहुमत ने ही उन्हें विमुद्रीकरण जैसे अनूठे उपाय लागू करने की ताकत दी है और इस बार शायद हमें चुनाव प्रणाली, विशेषकर राजनीतिक दलों और चुनावों के लिए धन के मसले पर सुधार के गंभीर प्रयास देखने को मिलें। किंतु ऐसे प्रयास तब अधिक विश्वसनीय होंगे, जब हम लोकपाल जैसी संस्थागत प्रणालियों को स्थापित करेंगे, जो चुनावों के लिए सरकारी धन जैसा ही प्रहरी हो सकता है।
(लेखक द पायोनियर में ओपिनियन एडिटर, वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार और लोक मामलों के विश्लेषक हैं)
Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)
Published Date: 16th December 2016, Image Source: http://voicesforfreedom.org

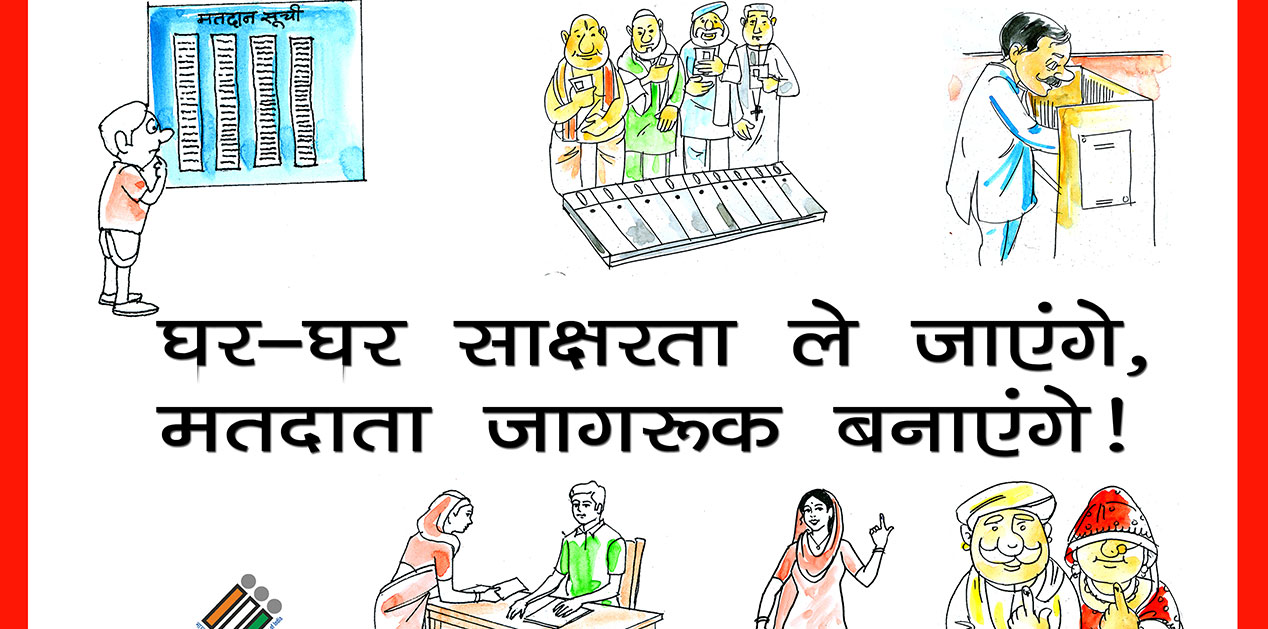









Post new comment