राष्ट्रपति चुनाव निकट हैं और तिनकों की तरह बिखरे विपक्षी दल एकजुट होने और इस पद के लिए संयुक्त प्रत्याशी तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बीजू जनता दल, ऑल इंडिया अन्नाद्रमुक और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से बाहर का लगभग प्रत्येक बड़ा दल अपनी पसंद का नया राष्ट्रपति बनवाने के लिए बातचीत करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राजग को अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। उनकी बातचीत से संकेत मिलता है कि उन्होंने दो बातें तय कर ली हैं। पहली, भाजपा की पसंद का विरोध करना ही करना है। दूसरी, भाजपा/राजग का प्रत्याशी गैर-धर्मनिरपेक्ष होगा। दोनों धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और उस गहराई तक जड़ जमाए और घिसे-पिटे पूर्वग्रह का नतीजा हैं, जो आइना दिखाए जाने के बाद भी चला आ रहा है।
भारत में धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों की सूची में सबसे ऊपर मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि “उनका दल ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनते देखना चाहता है, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि वाला हो, सांप्रदायिक दृष्टि वाला नहीं।” चूंकि उन्हें यकीन है कि भाजपा में सांप्रदायिक प्रत्याशी चुनने की न तो क्षमता है और न ही इच्छा, इसीलिए वह और समवैचारिक दलों को एक साथ आना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी “धर्मनिरपेक्ष गठबंधन” का समर्थन करने की बात कह दी है, हालांकि उन्हें उस नए धर्मनिरपेक्ष मोर्चे से समस्या है, जो उनके चाचा शिवपाल यादव ने बनाया है! अन्य नेता भी समर्थन कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी अपने कम्युनिस्ट प्रतिद्वंद्वियों से हाथ मिलाने तक को तैयार हैं, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) के शरद यादव ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपति’ का चुनाव सुनिश्चित कर देश और संविधान को “बचाना” चाहते हैं।
धर्मनिरपेक्षता मजबूत जोड़ है, लेकिन इसकी मजबूती बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आजादी के बाद से ही इसने सराहनीय काम किया है और मार्क्सवादियों, मध्यमार्गियों तथा समाजवादियों ने इसका पूरा फायदा उठाया है। वे दो प्रमुख कारणों से ऐसा कर पाए हैं। पहला, उन्हें किसी सार्थक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा और इसीलिए उन्हें एकदम खाली मैदान मिल गया। दूसरा, उन्होंने ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द को अपने राजनीतिक/चुनावी एजेंडा के हिसाब से अच्छी तरह तोड़ा-मरोड़ा और उसे राष्ट्र का सांस्कृतिक गुण बताकर पेश कर दिया। लेकिन इन दलों के लिए यह वैचारिक मुद्दा कभी नहीं रहा, हालांकि वे इस आरोप का विरोध करेंगे। समाजवादी और मध्यमार्गी इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए 1977 के जनता पार्टी प्रयोग के दौरान ‘सांप्रदायिक दक्षिणपंथियों’ के साथ एकजुट हो गए थे। 12 वर्ष बाद मार्क्सवादियों और दक्षिणपंथियों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनकी जनता दल सरकार का समर्थन करने के लिए हाथ मिला लिए। और भी उदाहरण हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भाजपा को गैर-धर्मनिरपेक्ष बताती है, वह केंद्र में भाजपानीत सरकार में शामिल थी। नीतीश कुमार का जनता दल (यूनाइटेड) भी उसी में था, जिसने बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार भी चलाई। इसलिए, जब ये दल आगामी राष्ट्रपति चुनाव को ‘वैचारिक संघर्ष’ बताते हैं तो हंसी आती है।
इस देश में धर्मनिरपेक्षता बहुत बड़ी जरूरत है, जिसमें सभी बुराइयों को छिपा देने की क्षमता है। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले कार्यकाल में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो उसने इस फैसले को यह कहकर सही ठहराया था कि सांप्रदायिकता (अर्थात् भाजपा) भ्रष्टाचार (जिसका प्रतीक कांग्रेस थी) से बड़ी बुराई है। नीतीश कुमार को भी ‘सांप्रदायिक भाजपा’ के साथ रहने के बजाय भ्रष्ट (और अपराधी) लालू प्रसाद से हाथ मिलाना अधिक स्वीकार्य था। ममता बनर्जी मार्क्सवादी हिंसा को भाजपा के गैर-धर्मनिरपेक्ष षड्यंत्र से कम खराब बताकर खारिज कर सकती हैं। और अगर सांप्रदायिक भाजपा को किनारे करने की बात आए तो कांग्रेस को शैतान के साथ दोस्ती करना भी स्वीकार है।
अगर धर्मनिरपेक्षता इतनी अधिक आकर्षक है और इस देश के नैतिक मूल्यों में इतनी ही रची-बसी है, जितनी ये दल बताते हैं तो धर्मनिरपेक्ष वर्ग चुनाव में बार-बार हार क्यों रहा है और भाजपा जीत क्यों रही है? क्या अधिकांश जनता सांप्रदायिक हो गई है और वह भी एकाएक हो गई है? ‘धर्मनिरपेक्ष’ कहते आए हैं कि भाजपा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिये चुनाव जीते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझा पाए हैं कि उसके जवाब में उनके प्रयास धराशायी क्यों हो गए। यदि वाकई वे इस मूर्खता भरी बात में यकीन करते हैं कि लोग सांप्रदायिक हो रहे हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए। फिर भी यह जानना रोचक है कि मतदाता धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं और पांच साल बाद सांप्रदायिक हो जाते हैं और बाद में एक बार फिर धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है। इसी तरह जब दल भाजपा के साथ जाते हैं तो सांप्रदायिक हो जाते हैं; जब वे उससे अलग हो जाते हैं तो एकाएक वे धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष अवसरवादी लोगों ने जो मुखौटा लगाया है, उसके पार देखने के लिए आपको अरस्तू जैसी मेधा की जरूरत भी नहीं है।
भारत में धर्मनिरपेक्षों का पतन धर्मनिरपेक्षता का पतन नहीं है। लोग अपने धार्मिक उत्सव पहले जितने उत्साह से ही मनाते हैं; वे एक दूसरे के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं; वे एक दूसरे को पहले जितनी ही गंभीरता से शुभकामनाएं देते हैं; दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ प्रेम और विवाह अब भी होते हैं - हालांकि यह आम बात नहीं है; एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता सही सलामत है। बेहद स्तब्ध करने वाली और संकट की परिस्थितियों में भी मानवता का बंधन बरकरार रहता है, जैसा दिल्ली में सिख-विरोधी हिंसा और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में हुए दंगों के दौरान दिखा था। सिख समुदाय के सदस्यों को हिंदू समुदाय के अराजक वर्गों ने निशाना बनाया था तो उन्हें आश्रय भी उसी समुदाय के लोगों ने दिया। हिंदू-मुस्लिम हिंसा में भी ऐसा ही होता आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख रहे हैं, उसके आसपास के अधिकतर हिस्से में मुस्लिम दुकानदार बिना किसी रुकावट के अपना कारोबार करते हैं। हाल ही में खबरें आई थीं कि मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के खिलाफ अपनी लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा की! नौशाद-शकील-रफी की तिकड़ी ने देश को कई यादगार भजन दिए हैं। हिंदू गायकों ने अल्लाह की प्रशंसा करने वाले गीत गाये हैं। ढेर सारे उदारहण हैं। भारत में मजबूत सूफी परंपरा है और “अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम” सबसे लोकप्रिय भजनों में शुमार रहा है, जो महात्मा गांधी को भी पसंद था।
यदि आज धर्मनिरपेक्षों को मुंह की खानी पड़ रही है तो इसका कारण उनका धर्मनिरपेक्षता का नकली पाठ है, जिसका अब पर्दाफाश हो गया है। लोग अब उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया गया और तुष्टिकरण ने समाज को बांट दिया। उसके कारण धीरे-धीरे रोष सुलगता रहा और सांप्रदायिक खूनखराबे के रूप में सामने आया। जब लोग टकराए तो उन्हें भड़काया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध ही उन्हें लड़वाया गया। ऐसे माहौल में सभी पक्षों के अनैतिक तत्व मौके का फायदा उठाते हुए हालात को बिगाड़ते रहे, स्वयंभू धार्मिक नेता दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगलते रहे। उन्हें कभी सीधे और कभी पीछे से राजनेताओं का समर्थन मिलता रहा और आज भी मिलता है क्योंकि वे उन्हें वोट बैंक मानते हैं। लेकिन अब खेल खत्म हो गया है या होने वाला है।
धार्मिक सहिष्णुता के लंबे इतिहास वाले इस देश में धर्मनिरपेक्षता लादने का फैसला सबसे मूर्खता भरे फैसलों में गिना जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं - जो बेहद बुद्धिमान और गंभीर थे और उनमें से कुछ उस धर्मनिरपेक्षता के हिमायती थे, जो आज चलन से बाहर हो रही है - को महसूस हुआ कि ऐसे देश के संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को केवल इसीलिए शामिल करना अनावश्यक है, जिसकी प्रकृति ही धर्मनिरपेक्ष है। फिर भी इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जुड़वा दिया। संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया था तो उसका चरित्र धर्मनिरपेक्ष ही था। इसे शामिल करने से देश की धर्मनिरपेक्ष छवि बढ़ने के बजाय नई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पहली समस्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ की परिभाषा से थी; संविधान में उसकी परिभाषा ही नहीं है। दूसरी समस्या यह थी कि भारतीय संदर्भ में राज्य एवं धर्म के बीच संबंध स्पष्ट ही नहीं है।
यदि प्रस्तावना में इसे जोड़ने के पीछे भारत को इस मायने में धर्मनिरपेक्ष बनाने की मंशा थी कि अलग-अलग धार्मिक आस्थाओं के बावजूद भारत भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि में एकसमान होगा तो यह मंशा एकदम अधूरी रही है। इसे नाकाम होना ही था क्योंकि बहुसंख्यकवादी और अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति के बीच टकराव बना ही नहीं रहा बल्कि बढ़ भी गया। तुष्टिकरण वाले खेमे की दलील थी कि बहुसंख्यकों की प्रधानता पर अंकुश लगाने और अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों की रक्षा करने के लिए देश के सामान्य कानून के बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ की जरूरत है। बहुसंख्यक समुदाय (आज उसे हिंदुत्व का खेमा कहा जाता है) ने इस बात पर जोर दिया कि धर्मनिरपेक्ष भारत में अलग-अलग नागरिकों के लिए धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून नहीं हो सकते। आजादी के बाद हिंदू पर्सनल लॉ में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया और उसे धर्मनिरपेक्षता का रंग देकर हिंदू कोड विधेयक लाया गया। लेकिन अधिकतर विधि-निर्माताओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी धर्मनिरपेक्षता का ऐसा ही रंग भरने की जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं हुई - 1949 में भी नहीं और आज भी नहीं। धर्मनिरपेक्षता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसके नाम पर मौलवियों द्वारा बताई गई हरेक बात, जिसमें तीन तलाक तथा बहुपत्नी प्रथा शामिल है, को जारी रखने के लिए ढाल का काम किया। आज हमें दिख रहा है कि इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई मुस्लिम समुदाय विशेषकर महिलाओं के बीच से ही शुरू हुई है। ये महिलाएं भी अड़ियल मौलवियों की ही तरह धार्मिक हैं, लेकिन वे मानती हैं कि इस्लाम में इन प्रथाओं की अनुमति नहीं है।
हमारी वामपंथी-उदार-समाजवादी-मध्यमार्गी सेना ने धर्मनिरपेक्षता के जिस विचार को बढ़ावा दिया है, वह बदनाम क्यों हुआ है, यह समझना तब आसान हो जाता है, जब कोई इस बुनियादी सच को स्वीकार कर लेता हैः जब कोई बाहरी वस्तु किसी शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है तो जैविक तंत्र फौरन सक्रिय हो जाता है और बाहरी वस्तु को खारिज करने या उससे लड़ने का तरीका तैयार कर लेता है। भारत में धर्मनिरपेक्षों ने देश की मूलभूत धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को अनदेखा कर धर्मनिरपेक्षता का पाश्चात्य नमूना लोगों पर थोपने का प्रयास किया। धर्मनिरपेक्षता की पाश्चात्य परिभाषा चर्च तथा सत्ता को अलग-अलग करती है, जिसकी भारत में कोई तुक ही नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ को किनारे रख दिया गया और अरुचिकर तथा अवांछित वस्तु को लोगों पर थोप दिया गया। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई और इंदिरा गांधी ने इसे संवैधानिक स्वीकार्यता प्रदान की। राजीव गांधी ने मुखौटा बनाए रखने की जरूरत भी नहीं समझी और एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला को गुजारा-भत्ता देने के उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील फैसले को अस्वीकार कर दिया तथा मुस्लिम समाज में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए संविधान में संशोध नही कर डाला। अपने पूर्ववर्तियों की ही तरह उन पर भी ओछी धर्मनिरपेक्षता का साथ देने की विवशता नहीं थी और यदि वह चाहते तो असली धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद कर सकते थे।
धर्मनिरपेक्ष देश वह होता है, जो किसी एक धर्म के दबदबे, धर्म के आधार पर दमन और धर्म के आधार पर बहिष्कार के विरुद्ध होता है। वह ऐसे राज्य से बिल्कुल उलट होता है, जो ईश्वर की सत्ता को मानता है अथवा जो औपचारिक रूप से एक या अधिक धर्मों पर चलता है। सदियों से जर्मनी और इंगलैंड ने प्रोटेस्टेंट धर्म का पालन किया है, जबकि इटली और स्पेन ने कैथलिक धर्म को बढ़ावा दिया है। आज कई मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां इस्लाम आधिकारिक धर्म है। नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र था; आज वह भी आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हो चुका है, हालांकि हिंदुओं की संवेदनाओं का वह पूरा सम्मान करता है। भारत की अधिकांश जनता हिंदू है, लेकिन प्राचीन काल से ही, जब बौद्ध और जैन धर्मों ने यहां जड़ जमाई थी, यह मूलतः धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। अगर हिंदू धर्म ने प्रभुत्व वाली ताकत होने का प्रयास किया होता तो देश में अन्य धर्मों का प्रसार नहीं हुआ होता और उसके परिणामस्वरूप दिख रहा अंतरजातीय सामंजस्य कभी विकसित नहीं होता। ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को प्रस्तावना में जोड़े जाने से पहले भी अनुच्छेद 25, 27 और 28 धार्मिक स्वतंतत्रता की गारंटी देते थे; जबकि अनुच्छेद 14, 15 और 29 के अंतर्गत नागरिकों को समानता प्राप्त थी, उनके धर्म कोई भी हों। पुनर्जागरण के पहले वाले पश्चिमी विश्व में राजा के जरिये चर्च के पाास संप्रभु सत्ता होती थी और राजा चर्च के प्रति निष्ठा रखता था। उस समय के पश्चिम के उलट भारत में कभी कोई धार्मिक संस्था अथवा प्रमुख नहीं रहा, जिसने राज्य के मामलों पर नियंत्रण रखा हो। पुनर्जागरण के उपरांत यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य बने और धर्मनिरपेक्षता का वह रूप फौरन भारत में मंगा लिया गया और पश्चिमी विचारों से अत्यंत प्रभावित नेहरू जैसे लोगों और इंदिरा गांधी ने उसका समर्थन किया।
धर्मनिरपेक्ष देश धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि धर्म को आधिकारिक दर्जा तो नहीं ही दिया जाता, उसे प्रशासन द्वारा न्यायोचित माने जाने वाले तरीकों से दबाया भी जा सकता है। या वह सभी धार्मिक मतों को स्वीकार करेगा और किसी एक को दूसरे की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं देगा। पहले प्रकार के विरुद्ध तर्क दिए जा सकते हैं और दूसरे प्रकार की व्यावहारिकता पर चर्चा हो सकती है। लेकिन तीसरे प्रकार की धर्मनिरपेक्षता में कुछ खूबी जरूर है। इस धर्मनिरपेक्षता को भारत पर मार्क्सवादियों-समाजवादियों-मध्यमार्गियों ने थोपा है और इसमें राज्य यह कहकर किसी धार्मिक समुदाय का पक्ष लेने लगता है कि वह अल्पसंख्यक तथा जरूरतमंद है। इसके बाद वह उस धर्म को विशेष स्थान दे देता है, जिसके कारण बहुसंख्यकों के साथ खुल्लमखुल्ला भेदभाव होने लगता है। बहुसंख्यक भावना का मुकाबला करने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति करना धर्मनिरपेक्षता नहीं है।
अंत में मार्क्सवादियों की ओर लौटें, जिन्होंने देश में स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का बड़ा पैरोकार घोषित कर रखा है। यह याद रखा जाना चाहिए कि उनके राजनीतिक संत कार्ल मार्क्स के पास धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति और परिभाषा पर विचार करने का समय ही नहीं था। बल्कि वह तो मानते थे कि धर्म श्रमिक वर्ग (सर्वहारा) को अभिजात्य (बुर्जुआ) वर्ग के खिलाफ एकजुट कर खड़ा करने की राह में बाधा है। अर्थ को आधार और संस्कृति, जातीयता, भाषा आदि शेष सभी को उस पर खड़ी इमारत मानने वाली उनकी आस्था में धर्म के लिए जगह ही नहीं थी। उन्होंने धर्म को उस वक्त भ्रम बताकर खारिज कर दिया, जब उन्होंने कहा, “धर्म लोगों के लिए अफीम है।” इसे सही संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि “वास्तविक प्रसन्नता के लिए आवश्यक है कि धर्म को लोगों की भ्रामक प्रसन्नता मानकर त्याग दिया जाए... इसलिए धर्म की आलोचना वास्तव में आंसुओं के उस गड्ढे की आलोचना है, जिसे धर्म की रोशनी से ढक दिया जाता है।” मार्क्स अपनी कब्र में यह देखकर तड़प रहे होंगे कि उनके चेलों ने भारत में अपने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह धर्म का दुरुपयोग किया है।
(लेखक द पायनियर में ओपिनियन एडिटर, वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार और लोक मामलों के विश्लेषक हैं)
Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)
Image Source: http://thecompanion.in

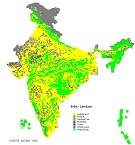









Post new comment